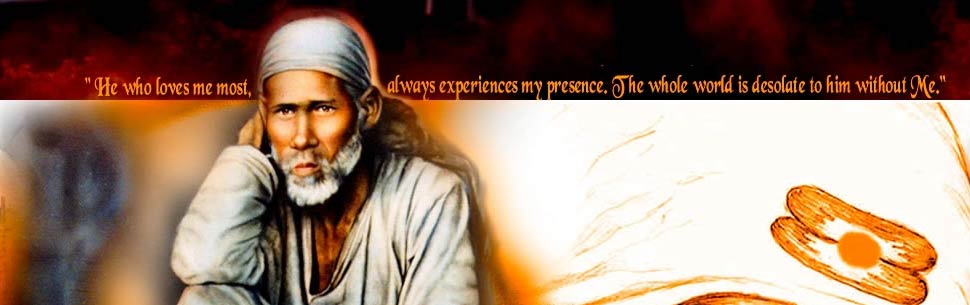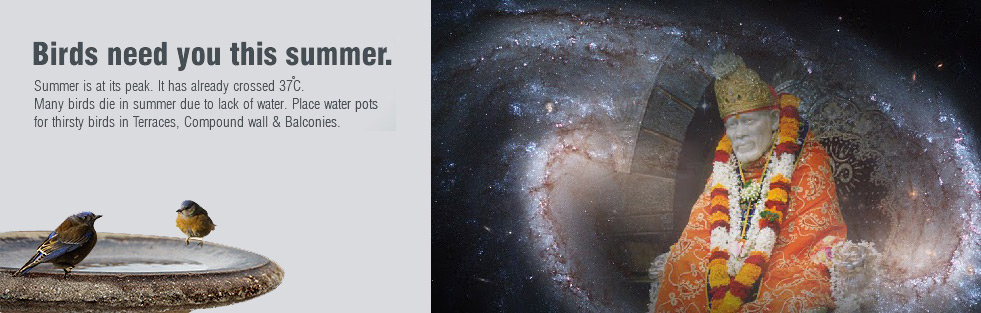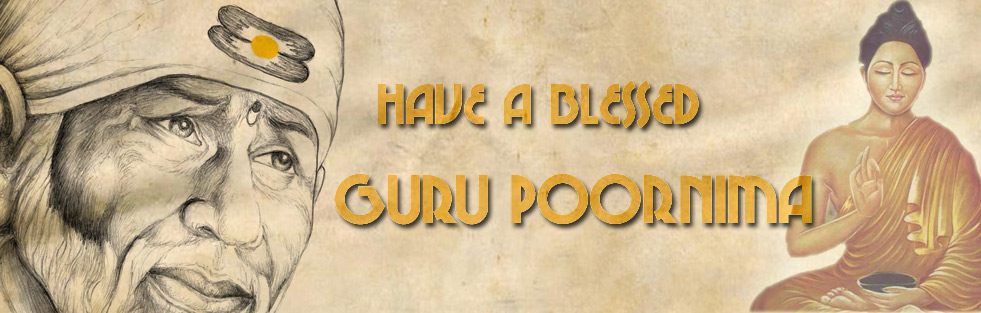ॐ श्री साईं नाथायनमः
जैसी भावना वैसी सिद्धि
भगवान सर्वव्यापक और शाश्वत हैं। वे सबको मिल सकते हैं। आप जिस रूप में भगवान को पाना चाहते हैं उस रूप में आपको मिलते हैं। श्रीकृष्ण गीता में भी वचन देते हैं किः
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।
'हे अर्जुन ! जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ।'
(गीताः 4.11)
आप कुशलता से परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं तो भगवान पदार्थों के रूप में मिलेंगे। आलसी और प्रमादी रहते हैं तो भगवान रोग और तमोगुण के रूप में मिलेंगे। दुराचारी रहते हैं तो भगवान नरक में मिलेंगे। सदाचारी और संयमी रहते हैं तो भगवान स्वर्ग के रूप में मिलेंगे। सूर्योदय के पहले स्नानदि से शुद्ध होकर प्रणव का जाप करते हैं तो भगवान आनन्द के रूप में मिलते हैं। सूर्योदय के बाद भी सोते रहते हैं तो भगवान आलस्य के रूप में मिलेंगे। भगवान की बनाई अनेक लीलाओं को, इष्टदेव को, आत्मवेत्ता सदगुरु को प्यार की निगाहों से देखते हैं, श्रद्धा-भाव से, अहोभाव से दिल को भरते हैं तो भगवान प्रेम के रूप में मिलेंगे। वेदान्त का विचार करते हैं, आत्म-चिन्तन करते हैं तो भगवान तत्त्व के रूप में मिलेंगे। घृणा और शिकायत के रूप में देखते हैं तो भगवान शत्रु के रूप में मिलेंगे। धन्यवाद की दृष्टि रखते हैं तो भगवान मित्र के रूप में मिलते है। अपने चित्त में सन्देह है, फरियाद है, चोर डाकू के विचार हैं तो भगवान उसी रूप में मिलते हैं। अपनी दृष्टि में सर्व ब्रह्म की भावना है, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दृष्टि आता है तो दूसरों की नजरों में जो क्रूर हैं, हत्यारे हैं, डाकू हैं, वे तुम्हारे लिए क्रूर हत्यारे नहीं रहेंगे।
आप निर्णय करो कि भगवान को किस रूप में देखना चाहते हैं। जब सब भगवान हैं, सर्वत्र भगवान हैं तो आपको जो मिलेगा वह भगवान ही है। समग्र रूप उसी के हैं। यह स्वीकार कर लो तो सब रूपों में भगवान मिल जायेंगे। आनन्द ही आनन्द चाहो, प्रेम ही प्रेम चाहो तो भगवान उसी रूप में मिलेंगे।
किसी को लगेगा कि जब सर्वत्र भगवान हैं तो पाप-पुण्य क्यों? फिर पाप करने में हर्ज क्या है?
हाँ, कोई हर्ज नहीं। डटकर पाप करो। फिर भगवान नरक के रूप में प्राप्त होंगे।
'सब ब्रह्म है तो जो आवे सो खाओ, जो आवे सो पियो, जो मिले सो भोगो, चाहे सो करो क्या हर्ज है?'
तो भगवान सर्वत्र हैं। वे रोग के रूप में प्रकट होंगे। संयम से रहोगे तो भगवान स्वास्थ्य के रूप में प्रकट होंगे।
भगवान हमारे समक्ष अपने समग्र रूप में प्रकट हो जायें ऐसी इच्छा हो तो अपने 'मैं' को खोजो। 'मैं' खो जाएगा फिर लगेगा कि भगवान समग्र रूपों में हैं और भी भगवत्तत्व था।
महायोगी श्री अरविन्द गीता के महान् उपासक थे। वे गीता के सत्यों को अपने जीवनरूपी साँचे में ढालने को पूर्णरूपेण कृतसंकल्प थे। वेदों और उपनिषदों का सार गीता है जिसे पढ़कर उन्होंने तीन प्रतिज्ञाएँ की थीं। राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर भारत माता को अँग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से मुक्त करना एवं आत्मसाक्षात्कार करना।
अलिपुर बम-कांड में उनकी धरपकड़ हुई और कारावास में डाल दिये गये। वहाँ पर भी उनकी योग साधना सतत चालू थी। रात-रात भर परमात्मा के ध्यान में मग्न रहते थे। श्री अरविन्द के बचाव पक्ष के बैरीस्टर श्री चित्तरंजनदास थे जिन्होंने फीस में एक पाई भी न ली थी (बाद में वे देशबन्धु दास के नाम से प्रसिद्ध हुए)। सरकार की ओर से सैंकड़ों प्रमाण और साक्षी खड़े किये गये थे जिनका खंडन करने के लिए उन्हें दिन रात श्रम करना पड़ता था। सालभर मुकद्दमा चला। एक दिन अंग्रेज न्यायाधीश के पास कड़े पुलिस बंदोबस्त तले श्री अरविंद को जेल में से अदालत लाया गया। देशभक्ति से चकचूर जनता ने न्यायालय को खचाखच भर दिया था। सरकारी वकीलों के समक्ष बेरीस्टर चित्तरंजनदास उपस्थित हुए। उस समय विद्युत-पंखे नहीं थे। विशाल चँवर से न्यायाधीश पर पवन डाला जा रहा था। चँवर डुलाने के लिए कैदियों का उपयोग किया जाता था।
सरकार कृतसंकल्प थी कि श्री अरविन्द को मुजरिम साबित कर फाँसी पर लटका दे और श्री अरविन्द शांतभाव से श्रीकृष्ण का चिन्तन किये जा रहे थे। उस समय उन्हें जो अनुभूति हुई वह अत्यंत रसीली एवं अदभुत थी। भगवान के समग्र स्वरूप का गीता वचन प्रत्यक्ष हुआ। श्री अरविन्दजी के ही शब्दों में इस प्रकार हैः
"मैंने न्यायाधीश की ओर देखा तो मुझे उनमें श्रीकृष्ण ही मुस्कराते दीखे। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने वकीलों की ओर देखा तो मुझे वकील दिखाई ही नहीं दिये, सब श्रीकृष्ण का रूप दिखाई दिये। वहाँ उपस्थित कैदियों की ओर निहारा तो सब कृष्णरूप धारण कर बैठे हुए दिखे। जगह-जगह मुझे श्रीकृष्ण का हूबहू दर्शन हुआ। श्रीकृष्ण मेरे सामने देखकर बोलेः 'तू बराबर देख। मैं सर्वव्यापी हूँ, फिर डर किस बात का?' उनके दिव्य दर्शन से, अभयदान प्रदान करती हुई उनकी वाणी से मैं संपूर्ण निर्भय हो गया। चिन्ता मात्र पलायन हो गई।" वर्षभर अदालत में मुकद्दमा चला। केस के अन्त में गोरे न्यायाधीश ने चुकादा दियाः 'निर्दोष'। लोगों के आनंद का पार न रहा। उन्होंने श्री अरविन्द को कन्धे पर बिठाकर आनंदोत्सव मनाते हुए प्रचण्ड जयघोष कियाः
"जय श्रीकृष्ण, जय श्री अरविन्द।"
समय की धारा में वह प्रसंग भी सरक गया, स्वप्न की नाई।
उमा कहौं मैं अनुभव अपना।
सत्य हरिभजन, जगत सब सपना।।
यह सपने जैसे संसार में सब समय की धारा में स्वप्नवत् हो जाता है। अतः जगत सब स्वप्न है। 'मैं आत्मरूप से सबका आधार सच्चिदानंद स्वरूप हूँ... सोऽहम्.... शिवोऽहम्.....' ऐसा चिन्तन करोगे तो भगवान ब्रह्म के रूप में प्रकट हो जाएँगे।
भोगी और विलासी को रोग होते हैं। विकारी जीवन में पश्चाताप, भय और चिन्ता होती है। भय, चिन्ता होवे तभी 'भगवान भय और चिन्ता के रूप में प्रकट हुए हैं' – ऐसा करके भय और चिन्ता से बाहर निकल जाओ। भगवदबुद्धि से भय को देखोगे तो भय दुःख नहीं देगा। भगवदबुद्धि से रोग और शत्रु को देखोगे तो रोग और शत्रु दुःख नहीं देंगे। भगवदबुद्धि से सुख और स्वर्ग को देखोगे तो वह सुख और स्वर्ग विषयासक्ति नहीं कराएँगे। कितने सुन्दर समाचार हैं!
आप भगवान को किसी रूप में प्रकट करना नहीं चाहते लेकिन भगवान जैसे हैं वैसा जमाना चाहते हैं, जैसे हैं वैसे ही देखना चाहते हैं।
जैसे हैं वैसे देखना चाहते हैं तो वे सब कुछ हैं। उनको सब कुछ जान लो, देख लो। नरक भी वे ही हैं, स्वर्ग भी वे ही हैं। रोग भी वे ही हैं और जो स्वास्थ्य भी वे ही हैं। धन्यवाद भी वे ही हैं, शिकायत भी वे ही हैं।
'हमको भगवान पूरे दिखने चाहिए।'
पूरा देखनेवाला कौन है, उसको पूरा खोजो। जो पूरा देखने वाले को पूरा खोज लेता है उसके अपने भीतर भगवान पूरे प्रकट हो जाते हैं।
खोजने में परिश्रम पड़े तो वे सब कुछ हैं ही ऐसा संतों का अनुभव मान लो न ! अपने को पूरा खोजोगे तो क्या होगा?
हेरत हेरत गयो कबीरो हेराई।
खोजते-खोजते खोजनेवाला खो जायेगा। 'मैं..... मैं....' करने वाला मिथ्या हो जायेगा। शेष ब्रह्म ही ब्रह्म रह जायेगा। नमक की पुतली गई समुद्र की थाह लेने। पुतली तो खो गई, हो गई सागर। ऐसे ही देह और अहंकार खो गया और रह गया केवल ब्रह्म। मिटी बूँद हो गई सागर। बूँद भी पानी है, सागर भी पानी है।
श्रीमद् आद्य शंकराचार्य ने करोड़ों ग्रन्थों का सार बताते हुए कहाः
श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः।
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः।।
अर्ध श्लोक कर कहता हूँ कोटि ग्रन्थ को सार।
ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या जीव ब्रह्म निरधार।।
जिसको मूल हम जीवात्मा बोलते हैं वह ब्रह्म अलग से नहीं है। जिसे हम तरंग बोलते हैं वह सागर से अलग नहीं। जिसे घटाकाश बोलते हैं वह महाकाश से अलग नहीं। जिसको हम जेवर बोलते हैं वह सोने से अलग नहीं। जिसे हम दो गज जमीन बोलते हैं वह पूरी पृथ्वी से अलग नहीं। दीवाल बाँध कर सीमा खड़ी कर सकते हो लेकिन अलग नहीं कर सकते हो लेकिन जमीन अलग नहीं कर सकते। 'हमारी जमीन..... तुम्हारी जमीन' ये मन की रेखाएँ खड़ी कर सकते हो लेकिन जमीन अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही 'हमारा शरीर.... तुम्हारा शरीर....' अलग मान सकते हो लेकिन दोनों की जो वास्तविक 'मैं' है उसे अलग नहीं कर सकते। घड़ों का अलगाव हो सकता है लेकिन घड़ों के आकाश का अलगाव नहीं हो सकता। चित्त के अलगाव हो सकते हैं लेकिन चित्त जिसके आधार से फुरते हैं उल चिदाकाश का अलगाव नहीं हो सकता। 'वह चिदाकाश आत्मा मैं हूँ'.... ऐसा ज्ञान कराने का भगीरथ कार्य वेदान्त का है। 'वास्तव मे तुम आत्मा हो, विश्वात्मा हो, परब्रह्म परमात्मा हो। मरने और जन्मने वाले पुतले नहीं हो' – ऐसा वेदान्त दर्शन फरमाता है। ॐ.... ॐ.....ॐ....
ऐसा ज्ञान पचाने वाला सिद्ध पुरुष शूली पर चढ़ते हुए भी निर्भीक होता है, रोते हुए भी नहीं रोता, हँसते हुए भी नहीं हँसता।
सन्तुष्टोऽपि न सन्तुष्टः खिन्नोऽपि न च खिद्यते।
तस्याश्चर्यदशां तां तां तादृशा एव जानते।।
'ज्ञानी पुरुष लोक दृष्टि से संतोषवान होते हुए भी संतुष्ट नहीं है और खेद को पाये हुए भी खेद को नहीं प्राप्त होता है। उसकी उस-उस आश्चर्य दशा को वैसे ही ज्ञानी जानते हैं।'
(अष्टावक्र गीताः 56)
तन सुकाय पिंजर कियो धरे रैन दिन ध्यान।
तुलसी मिटै न वासना बिना विचारे ज्ञान।।
करोड़ों वर्ष की समाधि करो लेकिन आत्मज्ञान तो कुछ निराला ही है। ध्यान भजन करना चाहिए, समाधि करनी चाहिए लेकिन समाधिवालों को भी फिर इस आत्मज्ञान में आना चाहिए। सेवा अवश्य करना चाहिए और फिर वेदान्त में आना चाहिए। नहीं तो, सेवा का सूक्ष्म अहंकार आयेगा। कर्तृत्व की गाँठ बँध जाएगी तो स्वर्ग में घसीटे जाओगे। स्वर्ग का सुख भोगने के बाद फिर पतन होगा।
वेदान्त का जिज्ञासु समझता है कि कर्मों का फल शाश्वत नहीं होता। पुण्य का फल भी शाश्वत नहीं और पाप का फल भी शाश्वत नहीं। पुण्य सुख देकर नष्ट हो जाएगा और पाप दुःख देकर नष्ट हो जाएगा। सुख और दुःख मन को मिलेगा। मन के सुख-दुःख को जो जानता है उसको पाकर पार हो जाओ। यही है वेदान्त। कितना सरल।
जिसको अपना बिछुड़ा हुआ प्यारा स्वजन मिल जाये, उसको कितना आनन्द होता है ! मेले में बिछुड़े बच्चे को माँ मिल जाये पत्नी को बिछुड़ा हुआ पति मिल जाये, मित्र को बिछुड़ा हुआ मित्र मिल जाये तो कितना आनन्द होता है !
जब अपना स्वजन कहीं मिल जाय तो इतना आनन्द होता है तो जिसको वेदान्त का ज्ञान हो जाता है उसको तो सर्वत्र अपना प्रिय प्रेमास्पद, अपना आपा मिलता है..... उसको कितना आनन्द मिलता होगा। ॐ....ॐ.....ॐ...
ॐ आनन्द ! ॐ आनन्द !! ॐ आनन्द !!!